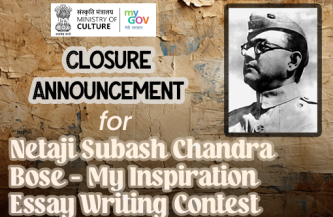सफ़लता के संकेत देती नई शिक्षा नीति
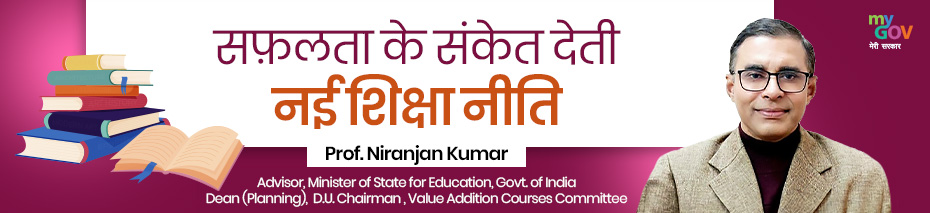
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अवतरण हुआ. नए सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को पूरे देश और दुनिया में सराहा गया. लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि महान विचार और धारणाएँ कार्य के बिना अर्थहीन हो जाते हैं , कुछ हलको में एनईपी-2020 के कार्यान्वयन को लेकर आशंका भी व्यक्त की गई. अब एनईपी-2020 के तीन वर्ष पूरे होने पर इसका लेखा-जोखा करना प्रासंगिक होगा. एनईपी का कार्यान्वयन कहाँ तक हो पाया? अब तक की क्या उपलब्धियां रहीं? और, भविष्य की क्या चुनौतियाँ हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के पहले यह समझना जरूरी होगा कि एनईपी-2020 के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं?
एनईपी-2020 अभिलेख का गहराई से पाठ करें तो इसके मूल में चार वैचारिक सरणियाँ कार्यरत दिखेंगी: भारतीयता ज्ञान परंपरा, महात्मा गाँधी का विजन, डॉ. आम्बेडकर का सामाजिक न्याय और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न. इन उच्च आदर्शों और विचारों को साकार करने के लिए, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के लिए, एनईपी में कुछ बुनियादी तत्त्व चिह्नित किए गए। इन तत्त्वों में एक गतिशील और समग्र दृष्टिकोण अंतर्निहित है जो सिद्धांत और अनुप्रयोग दोनों को सीखने पर समान रूप से जोर देता है। इसके अतिरिक्त बहुभाषावाद पर जोर और मानवीय मूल्यों का समावेश एवं छात्रों का समग्र विकास इस नए दृष्टिकोण के दो उल्लेखनीय पहलू हैं।
भारत की विशालता और विविधता को देखते हुए एनईपी को क्रियान्वित करना सचमुच आसान नहीं था। इन तत्वों को धरातल पर लागू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य हितधारकों के समग्र प्रयास से इसको चरणों में लागू किया जाना शुरू हो गया है. लेकिन देश के अनेक विश्वविद्यालय इस संदर्भ में अभी भी पीछे हैं, बल्कि कइयों को ठीक से अभी पता ही नहीं कि क्या करें और क्या न करें. उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एनईपी-2020 के कार्यान्वयन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अग्रणी भूमिका ले ली है. अपने कुलपति प्रो. योगेश सिंह के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एनईपी-2020 को शब्द और भाव दोनों ही स्तरों पर व्यवस्थित, संगठित और समग्र तरीके से लागू किया है जो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है. पहले चरण में डीयू ने यह कार्यान्वयन स्नातक स्तर पर किया है और अब अगले चरण की तैयारी चल रही है.
लचीलापन एनईपी-2020 की एक प्रमुख विशेषता है ताकि अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप शिक्षार्थियों को अपने सीखने के पथ और पाठ्यक्रम चुनने के अवसर हों. इस संदर्भ में डीयू के नए करिकुलम फ्रेमवर्क को देखें तो छात्रों को न केवल अपने रूचि के विषय के अन्दर कोर्सेस चुनने का अधिकार है बल्कि सामान्य ऐच्छिक ( general elective) कोर्सेस में वह किसी दूसरे स्ट्रीम से भी कोर्स पढ़ सकेगा. अर्थात विज्ञान वाला सामाजिक विज्ञान- मानविकी से भूगोल या संगीत अथवा वाणिज्य से मैनेजमेंट या मार्केटिंग के कोर्स पढ़ सकता है. अर्थात रूचि के विषय के विशेष ज्ञान के साथ-साथ बहु-विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर होंगे ताकि विद्यार्थी में समग्र दृष्टि विकसित हो सके. पूरे पाठ्यक्रम को इस तरीके से विन्यस्त किया गया है कि हर वर्ष की पढ़ाई अपने में पूर्ण है. किसी कारणवश कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ना चाहे तो डीयू एक साल बाद उसे सर्टिफिकेट और दो वर्ष बाद उसे डिप्लोमा दे देगा. यही नहीं, एक बार छोड़कर जाने के बाद वापस आकर अपनी बची पढ़ाई को पूरा करने का अवसर भी डीयू देगा.
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु एनईपी-2020 कौशल विकास और रोजगारपरकता पर बहुत बल देता है. डीयू में हर स्ट्रीम के विद्यार्थी को कौशल शिक्षा मिलेगी. सौ से ज्यादा स्किल कोर्सेस हैं जो हमारे युवाओं के स्वरोजगार की दिशा में सहायक होंगे. इसके अलावा एक नई और बड़ी बात यह है कि अबतक मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट आदि के छात्रों को उपलब्ध इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट आदि के अवसर डीयू में परंपरागत प्रोग्राम में भी उपलब्ध हैं जो उनके अनुभवजन्य (empirical) ज्ञान को बढ़ाएगा. यही नहीं, उद्यमिता (entrepreneurship) भी अब डीयू करिकुलम का हिस्सा है. विद्यार्थी एक उद्यम खड़ा करे, डीयू उसे एक कोर्स के रूप में मानकर क्रेडिट यानि अंक देगा.
बहुभाषावाद एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है. डीयू इस क्षेत्र में भी अग्रगामी है. संविधान के अनुच्छेद 8 में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओँ का अध्ययन-अध्यापन आरम्भ हो चुका है. ‘भारतीय भाषाओँ के अध्ययन-अध्यापन’ के साथ-साथ एनईपी ‘भारतीय भाषाओँ में अध्ययन- अध्यापन’ पर भी जोर देता है. न केवल मानविकी- सामाजिक विज्ञानों में बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढाई के लिए भी. इस संदर्भ में तो डीयू ने एक बड़ी राष्ट्रीय सेवा की है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘स्वयम’ पोर्टल के लिए तैयार किए गए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को भारतीय भाषाओँ में रूपांतरित करने में डीयू की महत्त्वपूर्ण भूमिका है.
राष्ट्र की उन्नति में शोध एवं नवाचार की अहम भूमिका को समझते हुए एनईपी में इसपर बहुत बल है. डीयू ने इस दिशा में भी एक बड़ी पहलकदमी की है. शोध एवं अनुसंधान डीयू में स्नातक स्तर पर ही करिकुलम का अब हिस्सा बन चुका है.
इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान और एनईपी में उल्लिखित सामाजिक न्याय की भावना को ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग जैसे अपने नए प्रोग्रामों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के एडमिशन के लिए डीयू ने फीस को बहुत कम रखा है. मिसाल के लिए 4 लाख रूपये तक के सालाना आय वालों को प्रवेश के समय फीस में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
लेकिन छात्रों और प्रकारांतर से राष्ट्र का समग्र विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि वे मानवीय-नैतिक मूल्य से परिपूर्ण और समग्र-संतुलित व्यक्तित्व न हों. पश्चिमी जीवन शैली, टेक्नॉलोजी में सिमटती दुनिया, रियल लाइफ के बजाय वर्चुअल लाइफ, शारीरिक खेलकूद की जगह गैजेट गेम्स, बढ़ते एकाकीपन आदि ने युवाओं को एक खतरनाक गिरफ्त में लेना शुरू किया है. दुष्परिणाम है ऐसे असंतुलित व्यक्तित्व का निर्माण जो समाज- देश के लिए अनुत्पादक, बोझ और कई बार खतरनाक साबित हो रहे हैं. शैक्षिक स्तर पर इनसे निपटने के डीयू की मूल्य संवर्धन समिति ने एकदम अभिनव पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है. छात्रों के चरित्र निर्माण तथा समग्र विकास और साथ ही उनमें भारतीय ज्ञान परम्परा एवं मानवीय मूल्यों का सम्यक संचार करने के लिए ऐसे ‘मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम’ (Value Addition Courses) बनाए गए हैं जिनमें गांधीवादी पद्धति का अनुसरण करते हुए 50 प्रतिशत अध्ययन व्यावहारिक और अनुभवजन्य है. यह बात न केवल विज्ञान की ओर उन्मुख पाठ्यक्रमों पर, बल्कि मानविकी/साहित्य पर आधारित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होती है. ये सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट कोर्स हैं, और साइंस, ह्यूमैनिटीज-सोशल साइंस और कॉमर्स सभी के छात्रों के लिए चार सेमेस्टर पढ़ना अनिवार्य है.
एनईपी रीस्किलिंग अर्थात पुनर्शिक्षण की बात भी करता है. इस संदर्भ में अपने योग्यता वृद्धि योजना (सीईएस) के तहत डीयू अधिक उम्र वालों को भी प्रवेश देगा जिससे वे स्वयं की योग्यता वृद्धि कर सकें. अध्यापन-शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनईपी में ‘क्लस्टर’ की परिकल्पना-योजना है जिसमें एक संस्थान के विद्यार्थी किसी विषय या कोर्स पढ़ने के लिए दूसरे संस्थान में जा सकेंगे. इस संदर्भ में भी डीयू ने पहल करते हुए विभिन्न कॉलेजों के लिए ‘क्लस्टर’ मॉडल बनाया है.
हालाँकि एनईपी के पूर्ण कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं. आर्थिक संसाधन की अपर्याप्तता, आधारभूत संरचना की समस्याएँ, शोध एवं विमर्श की भारतीय दृष्टि का अभाव, शोध के अहम पड़ाव पीएचडी में एडमिशन प्रक्रिया की सीमाएँ, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय आदि कई बिंदु हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना होगा.
पर समग्रता में देखें तो छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए निर्मित एनईपी-2020 का कार्यान्वयन डीयू ने श्रेष्ठ तरीके से किया है. यह देश के अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए एक आदर्श साबित होगा, इसमें संदेह नहीं.
[प्रो॰ निरंजन कुमार; दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन (योजना) और एनईपी सेल के सदस्य हैं. पूर्व में वे अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक रहे हैं.